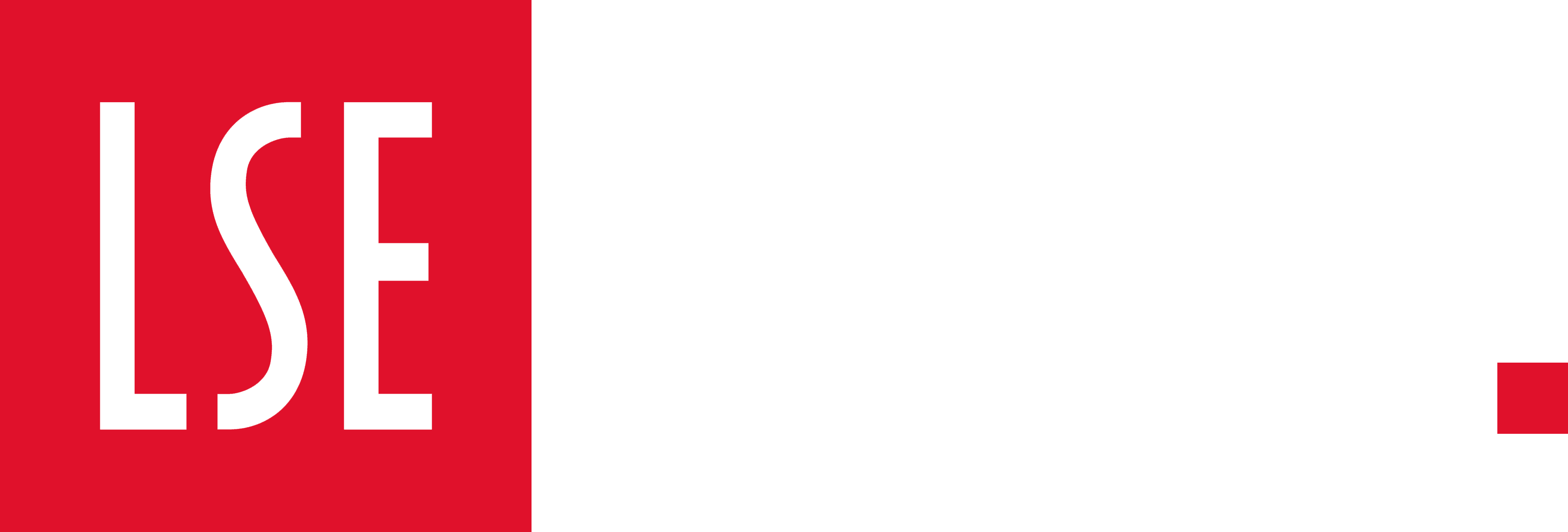“रिवीलिंग इंडियन फिलैंथ्रोपी” पढ़ने के बाद, फ्रांसेस्को ओबिनो का सवाल है कि क्या भारत में लोकोपकार(फिलैंथ्रोपी) समतामूलक तथा टिकाऊ विकास में मददगार हो सकता है ।
Click here to read this post in English.
भारत में घरेलू लोकोपकार की बढ़ती हुई क्षमता आशा जगाती है। भारतीय करोड़पतियों की संख्या 2012 में एक लाख तिरपन हजार (यूएस डॉलर के आधार पर) थी और अनुमानों के मुताबिक साल 2017 तक यह संख्या दो लाख बयालीस हजार तक पहुंच जायेगी जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। साल. उम्मीद है कि साल 2025 तक मध्यवर्ग के लोगों की तादाद भी भारत की आबादी में40 फीसद से लेकर 66 फीसद यानि 50 करोड़ से एक अरब के बीच हो जायेगी। भारत के नव-संभ्रांत तथा मध्यम वर्ग, दोनों सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करने के लिहाज से दान-कर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा,हाल में भारतीय कंपनी बिल में संशोधन करते हुए भारत के बडे व्यवसायिक उद्यमों के निवल लाभ के दो फीसद हिस्से को कारपोरेट के सामाजिक उत्तरदायित्व (कारपोरेट सोशल रेस्पांस्बिलिटी) के मद में नियत किया गया है। इससे सालाना 1 से 2 अरब डॉलर(यूएस) की अतिरिक्त आमदनी होगी।
कुछ लोग शीर्ष पर और बढ़ते हुए क्रम से ज्यादातर जन तल पर- भारत में भी आय-वितरण की संरचना विकसित देशों के समान लगातार पिरामिडनुमा होती जा रही है। साथ ही, आर्थिक-वृद्धि की रफ्तार तेज है। इन वजहों से भारत में लोकोपकार प्रवृत्त लोगों की कुल संख्या बढ़कर, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की सम्मिलित जनसंख्या से कहीं ज्यादा हो सकती है, और वह भी दो दशक से कम समय में। भारतीय नागरिकों तथा व्यवसायियों में भारत के विकासपरक कामों के लिए दानदाता बनकर उभरने की प्रभूत संभावनायें हैं।
लेकिन उम्मीद ऊंची हो तो उसे थामने के लिए सावधानी बहुत जरुरी हो जाती है। यदि लोकोपकार को, जैसा क, भारत के विकास के एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में उभरना है तो इस बात की बेहतर समझ बहुत जरुरी है कि कितना धन उपलब्ध होगा तथा उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यह मानें कि निजी दान में हुई आकस्मिक वृद्धि बहुत हाल की घटना है, और यही रुझान लंबी अवधि तक जारी रहेगा ऐसा अनुमान लगाना एक हड़बड़ी है, तो फिर यह सवाल बरकरार रहता है कि भारत में घरेलू लोकोपकार विकास के मोर्चे पर चुनौतियों से निपटने में वास्तविक रूप से कैसे और क्या योगदान कर सकता है।
इस सवाल की रोशनी में देखें तो यूबीएस तथा एलएसई के इंडिया ओब्जर्वेटरी द्वारा मैथ्यू कैंटेग्रील, द्वीप चनाना, तथा रूथ कट्टुमुरी के संपादन में निकली पुस्तक “रिवीलिंग इंडियन फिलैंथ्रोपी” का हालिया लोकार्पण बड़ा समयानुकूल कहा जायेगा ।
किताब में लोकपकार के लिए प्रसिद्ध कुछ भारतीयों के व्यक्तिगत अनुभवों को तरतीब से रखते हुए संपादकों ने लोकोपकारिता के उद्भव, उद्देश्य और दिशा के बारे में छोटे-छोटे आख्यानों के सहारे भारत में लोकोपकार के इतिहास का ताना-बाना बुना है। यह पुस्तिका भारतीय लोकोपकार की विविधिता की चर्चा करते हुए उसके तौर-तरीके और दृष्टिकोण को समझाती है साथ इस संदर्भ में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर भी प्रकाश डालती है।
जो विशाल संपत्ति के मालिक हैं वे सामाजिक प्रयोजन के निमित्त ट्रस्ट या फिर फाऊंडेशन बनायें- अमेरिका में लोकोपकार के लिए प्रसिद्ध कार्नेगी तथा रॉकेफेलर ने 19 वीं सदी अंतिम वर्षों में इसी को एक मॉडल के रुप में ‘वैज्ञानिक लोकोपकार'( साइंटिफिक फिलांथ्रोपी) का नाम दिया था। किताब की अन्तर्धारा इस मॉडल को एक संभावना के तौर पर उकेरती हुई आगे बढ़ती है । संपादकों ने किताब में कुछ ऐसे बड़े घरानों तथा व्यक्तियों लोकोपकारियों की बढ़ रही एक नई पीढ़ीकी पहचान की है जिनका दान-कर्म आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक रहा है। साथ ही किताब में लोकोपकार में प्रवृत्त उभर रही नई पीढ़ी को भी लक्ष्य किया गया है। किताब से जो चित्र उभरकर सामने आता है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत में ऐसे अमीर लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है जो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा विद्यालयों, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थानों, के निर्माण तथा आवास और भोजन वितरण के बेहतर कार्यक्रमों में लगाकर देश के विकास में सहायक बनने के लिए उत्सुक हैं।
यह पुस्तक भारत में विद्यमान लोकोपकार की परंपरा का तो विश्वसनीय चित्रण करती है लेकिन इस जरुरी सवाल से पर्याप्त मुठभेड़ नहीं करती कि लोकोपकार को समताकारी और टिकाऊ विकास के काम में कैसे परिणत किया जाय।
मानव-विज्ञानी एरिका बोर्नस्टीन ने, नई दिल्ली में लोकोपकारिता पर केंद्रित अपने एक अध्ययन (2009) में जैक डेरिडा के ‘शुद्ध उपहार’ की धारणा से मार्शल मौश की उपहार संबंधी धारणा का अन्तर दिखाया है। शुद्ध उपहार की धारणा मानती है कि दान-कर्म किसी भी दायित्व-बोध, अधिकार-भावना या फिर दाता और ग्रहीता के बीच के संबंध से परे है जबकि मार्शेल मौस के अनुसार दान-कर्म में लेन-देन का व्यवहार शामिल है, इसमें पारस्परिकता होती है और यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संबंध का अनिवार्य अंग होता है। बॉर्नस्टीन का तर्क है कि भारत में दान-कर्म को अहैतुक दान( बॉर्नस्टीन ने इसे हिन्दुओं के बीच प्रचलित धार्मिक संस्थाओं को दान देने की प्रथा से जोड़ा है) तथा समाज की भलाई की इच्छा के बीच मौजूद तनाव के सहारे समझा जाना चाहिए।
परस्पर विरोधी इन दो ध्रुवों के बीच ‘वैज्ञानिक लोकोपकार’ का विचार सहजता से फिट होता नहीं जान पड़ता। लोकोपकार की योजना चाहे कितनी भी बारीकी से बनायी गई हो और चाहे उसपर कितनी भी बेहतरी से अमल किया गया हो- अपने आप में वह निजी कर्म ही है। बैंक इसी कारण लोकोपकार को वैयक्तिक निवेश कहकर प्रचारित-प्रसारित करते हैं। पुस्तक में शामिल कुछ रचनाकारों में इस बात का स्पष्ट बोध है कि लोकोपकार विकास-कार्य में योगदान देने वाले शेष कारकों की जगह नहीं ले सकता बल्कि वह विकास कार्य के शेष कारकों का अनुपूरक होता है जबकि पुस्तक में शामिल शेष रचनाकार इस फांस की लपेट में आ गये हैं और उन्होंने वैयक्तिक दान-कार्य को स्वयंसेवी संगठनों या फिर राजसत्ता के दोषपूर्ण प्रयासों के बरअक्स ऱखकर देखा-समझा है।
किताब में जो हिस्सा आंखो-देखी(फर्स्टहैंड अकाऊंट) की शक्ल में लिखा गया है वह गरीबी और विकास को ना तो राजनीतिक मसला मान पाता है और ना ही यह स्वीकार करता है कि इन मसलों का समाधान (धीमी प्रगति के कारण) लंबे जुड़ाव की मांग करता है। किताब के इस हिस्से में शायद ही कहीं यह समझ दिखायी देती है कि गरीबी और विकास के मसले सामाजिक और राजनीतिक कारकों को लक्षित होते हैं जिनकी अपनी अलग आवाज होती है। लोकोपकार में प्रवृत्त लोग यह मानने से कतराते हैं कि वे खुद भी समस्या और उसके समाधान का ठीक उसी तरह एक हिस्सा हैं जिस तरह वे लोग जिनकी सहायता के लिए वे प्रयासरत रहते हैं।
भारत की व्यवस्थागत असमानता और गरीबी को दूर करने में लोकोपकार प्रवृत्त लोगों की भूमिका को विकास-कार्य में लगे अन्य कारकों से समन्वय तथा विकासपरक व्यापक बहस का अभाव अत्यंत सीमित कर सकता है। ठीक इसी तरह किसी लोकोपकारी के निजी राजनीतिक झुकाव पर निर्भर दिशा-दृष्टि (चाहे यह भौगोलिक हो या विषयगत) भी उसके प्रयासों को सीमित करने वाला साबित हो सकती है।
भारत में समृद्धि और निर्धनता साथ- साथ मौजूद हैं और यह मौजूदगी अपने आकार और परिमाण के लिहाज से एक अद्वतीय घटना है – ऐसा कहना कोई नयी बात कहना नहीं है। बहरहाल, यह दावा कि भारत के धनिकों में बढ़ रही लोकोपकारिता की संस्कृति भारत की विकासपरक चुनौतियों से निबटने में लगातार मददगार साबित होगी- एक नई बात में गिना जा सकता है। जीडीपी के तेज विकास दर के बावजूद विकासपरक चुनौतियां बढ़ रही हैं।इसे नजर में रखते हुए भारत में लोकोपकारिता के बाजार की संभावनाओं पर तत्काल ध्यान देने की जरुरत है। “रिवीलिंग इंडियन फिलैंथ्रोपी“ भारत के विकास तथा इसके उत्प्रेरकों की वृहतर बहस में लोकोपकार के विषय का सूत्रपात करने में मददगार साबित होगी लेकिन जरुरत इस बात की है कि जो कुछ पहले से किया जा चुका है, उसके गुणगान तक सीमित ना रहकर बहस को आगे बढ़ाया जाय।