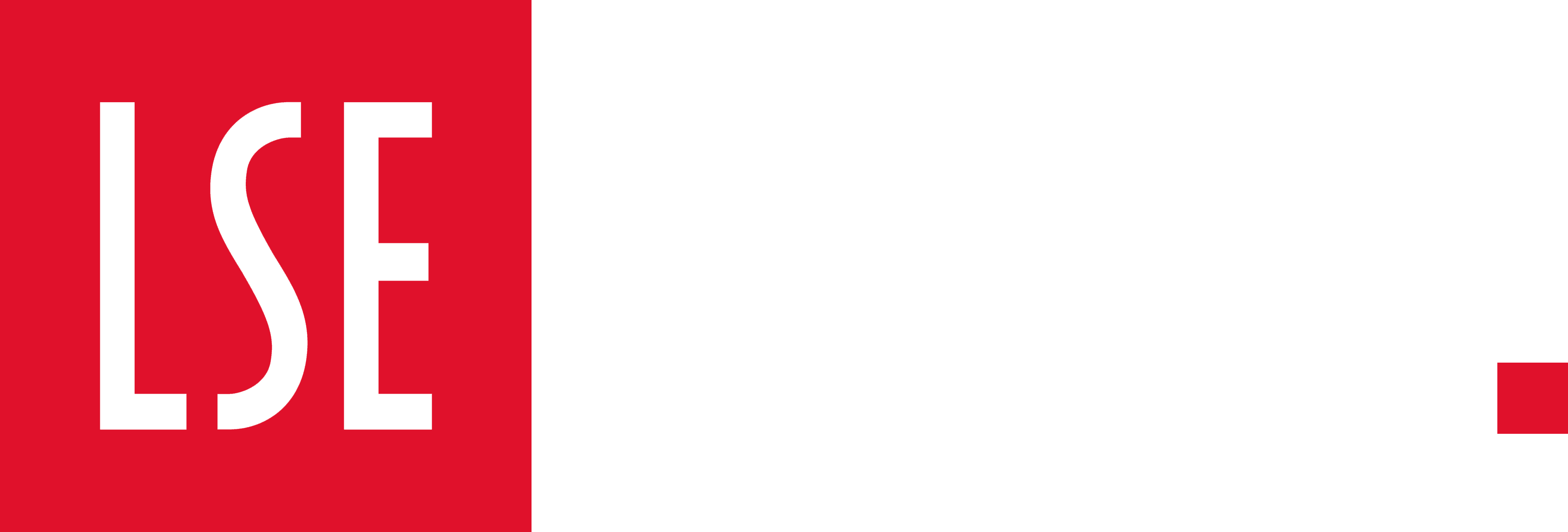पॉलिटिकल जियोग्राफी के एक विशेषांक, ‘ ज्यॉग्राफी ऐट दी मार्जिन्स्: बॉर्डर्स इन साऊथ एशिया” से परिचय करवाते हुए इस आलेख में रोमोला सान्याल का कहना है कि दक्षिण एशिया के इतिहास और वर्तमान को समझने के लिहाज से इस क्षेत्र की सीमा-रेखाओं का केंद्रीय महत्व की हैं।
Click here to read this post in English.
इस विशेषांक की शुरुआत दक्षिण एशिया में सीमा-रेखाओं द्वारा ग्रहण किए गए अलग-अलग अर्थ और स्वरूप को जानने की कोशिश के रुप में हुई। कोशिश यह भी रही कि सीमा-रेखाओं के इतिहास और भूगोल का विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन किया जाय जो संबंधपरक भी हो और तुलनात्मक भी। दक्षिण एशिया ऐसे अध्ययन के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र है। एक तो इसलिए कि यहां अनगिनत सीमा-रेखाएं मौजद हैं। दूसरे, दक्षिण एशिया के इतिहास के अधिकतर हिस्से का वर्णन , चाहे यह औपनिवेशिक काल का हो या उत्तर-औपनिवेशिक काल का, सीमान्तों और सीमा-रेखाओं के निर्माण को प्रस्थान बिन्दु मानकर किया जा सकता है।
और एक बात यह भी है कि मौजूदा दक्षिण एशिया की सीमा-रेखाएं आपस में गुंथी-बिंधी हैं और एक-दूसरे को प्रतिस्थापित करते रहती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां राष्ट्रों के सीमांत पर सामुदायिक विभाजनों का राग बजता है तो उसकी अनुगूंज शहरी क्षेत्रों में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की तरह दर्ज होती है। एक ऐसा स्थान, जहां सीमा सुरक्षा बल नेशनल पार्कों की सीमाओं पर पहरेदारी करते हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा-रेखाओं के आर-पार लोगों की आवाजाही स्वयंसेवी संगठनों की निगरानी में होती है। दक्षिण एशिया में एक तरफ जहां राष्ट्रीय इतिहास को उत्तर-आधुनिक इतिहास ने नये सिरे से परिभाषित किया है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय अस्मिताओं का वर्गीकरण यहां की भौगोलिक सीमा-रेखाओं की संकीर्णता से कहीं आगे बढ़कर किया गया है। इसलिए दक्षिण एशिया के इतिहास और वर्तमान को समझने के लिहाज से उसकी सीमारेखाओं और सीमान्तों को समझना केंद्रीय महत्व का है।
सीमा-क्षेत्रों में हाशिया पर होने की स्थितियां कई अर्थ ग्रहण करती हैं। अंक में शामिल लेखकों ने इन विभिन्न अर्थों को खोजने के लिए कई मुद्दों पर ध्यान दिया है। अंक के लेखकों ने साक्ष्यों से भरपूर विश्लेषण के जरिए सीमान्तों पर सक्रिय प्रक्रियाओं की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की है और सिद्धांत के धरातल पर इन प्रक्रियाओं को हाशियाकरण, विस्थापन, उत्तर-आधुनिक सैद्धांतिकी और प्रतिस्पर्धी इतिहास के व्यापक दायरे में चिह्नित किया है।
हमारा यह विशेषांक दो तर्कों को उठाता है। पहला, हम क्षेत्र की समझ, उसके सीमान्तों और सीमा-रेखाओं पर ध्यान केंद्रित करके, विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमारा तर्क है कि नगरीय और राजनीतिक भूगोल से संबद्ध साहित्य के बीच(और इससे इतर भी) संबंध को अवधारणा के धरातल पर कहीं ज्यादा सुस्पष्ट तरीके से जोड़ने की जरुरत है। सीमारेखा के विशिष्ट इतिहासों के विवेचन के जरिए हमारा लक्ष्य उन सिद्धांतों तक पहुंचना है जो राष्ट्रों और राज्यसत्ताओं के कहीं ज्यादा बड़े मुद्दों से इन सीमारेखीय इतिहासों के तकलीफदेह रिश्तों को चिह्नित कर सकें।
विशेषांक पाँच शोध-पत्रों का संग्रह है। ये शोधपत्र डॉ. जेसन कॉन्सकॉन्स (बकनेल यूनिवर्सिटी), डॉ. सारा श्नाइडर्मन (येल यूनिवर्सिटी), डॉ. टाउसेंड मिडलटन (ड्युक यूनिवर्सिटी), डॉ. सारा स्मिथ (यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलाइना, चेपल हिल) और डॉ. क्रिस्टीना हैरिस (यूनिवर्सिटी ऑफ एम्सटर्डम) ने प्रस्तुत किए हैं। साथ ही विशेषांक में डॉ. कॉन्सकॉन्स और मेरे द्वारा लिखी गई एक भूमिका शामिल है जो विशेषांक के सैद्धांतिक तर्कों को रेखांकित करती है। विशेषांक के शोधपत्र नागरिकता, व्यापार, सीमा-पारीय आवाजाही, प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) जैसे मुद्दों और भारत, बांग्लादेश, तिब्बत, लद्दाख और नेपाल के बीच सीमाओं के पास बदलते जातीय संबंधों का विश्लेषण करते हैं।
कॉन्स ने भारत-बांग्लादेश सीमा के पास के विदेश अंत:क्षेत्रों (एंक्लेव) के अपने अध्ययन में जोखिम की विषयवस्तु को उठाया है। शहरी झुग्गियों पर किये गये अध्ययनों की सैद्धांतिक प्रस्थापनाओं के आधार पर कॉन्स अपने तर्क से एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव करते हैं जो बांग्लादेश की नागरिकता के बारे में दाहाग्राम के निवासियों के दावे के प्रति सजग हो, साथ ही इन दावों की काट में खड़े विरोधपरक इतिहास के प्रति भी उसमें सजगता हो। कॉन्स ने अपने शोधपत्र में दाहाग्राम के निवासियों के दावों का विश्लेषण किया है। इन दावों की बनावट बहुभंगी है। साथ ही कॉन्स ने उन लोगों के समावेशन के दावों को अपने विश्लेषण में शामिल किया है जो राष्ट्रीय संबद्धता की मूल्यपरक धारणाओं के दायरे में नहीं आते। कॉन्स के विश्लेषण में वैसी आवाजें भी शामिल हैं जो जमीन, हाशियाकरण और राष्ट्र विशेष की सदस्यता के बारे में अलग किस्म की संवेदनशीलता का परिचय देती हैं। इन तमाम बातों के विश्लेषण के सहारे वह उन तरीकों का निदर्शन करते हैं जिसके द्वारा सीमान्त क्षेत्र के समाज की आंतरिक राजनीति, सीमा-रेखा की अधिक व्यापक राजनीति के संदर्भ में स्वयं को गढ़ती हैं। साथ ही उनका विश्लेषण बांग्लादेश में नागरिकता की नृवंशीय-राष्ट्रवादी समझ के साथ संवाद कायम करता है।
श्नाइडर्मन ने नेपाल और चीन के बीच के हिमालयी सीमा-क्षेत्र और नेपाल-चीन सीमा के भीतर 30 किलोमीटर के दायरे में निवासियों की निर्बाध आवाजाही का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन में हम देखते हैं कि किस तरह सीमान्त का एक क्षेत्र ऐसे लोगों का निर्माण करता है जो राजनीतिक और स्थानिक धरातल पर अपने हाशिये की स्थिति को खुद के अनुकूल बनाने में सक्षम हैं और सीमान्त पर होने की अपनी दुर्लभ स्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। राज्य नागरिकता के वैकल्पिक रुपों की रचना करते हैं- श्नाइडर्मन का अध्ययन इस बारे में एक अनूठी सूझ प्रदान करता है। नेपाल और चीन के बीच के हिमालयी सीमा-क्षेत्र के मामले में देखते हैं कि सीमान्त-क्षेत्र की नागरिकता दक्षिण एशिया और विश्व में राज्य-निर्माण और नागरिकता की प्रचलित प्रक्रियाओं के विपरीत काम कर रही है। श्नाइडर्मन का कहना है कि राज्यों को बाध्य होकर ऐसा करना पड़ता है। ऐसा जमीनी स्तर पर मौजूद जीवन-व्यवहारों को देखते हुए करना पड़ता है। ये जीवन-व्यवहार सीमारेखा के नियंत्रण और उसके आर-पार होने वाली आवाजाही की प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं।
मिडलटन ने अपने शोध-आलेख में दिखलाया है कि भारत का अलग-थलग पडा एक क्षेत्र दार्जिलिंग अस्मिताओं और अस्मितापरक राजनीति को रुपाकार देने के कारण किस तरह राजनीतिक रुप से हाशियाकरण की स्थिति उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण साधन की तरह काम कर रहा है। यहां, गोरखा लोग अपनी एक अलग पहचान निर्मित करने और भारतीय सरकार से मान्यता प्राप्त करने के लिए सतत संघर्षशील हैं, लेकिन भारत में अस्मिता को मान्यता प्रदान करने का एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है और यह परिप्रेक्ष्य गोरखा लोगों की अस्मितापरक मान्यता के संघर्ष को रूपांतरित, सीमित या फिर बाधित करता है।
लद्दाख पाकिस्तान और तिब्बत की सीमाओं से लगता दूर-दराज का एक विरोधग्रस्त क्षेत्र है और स्मिथ ने अपने शोध-आलेख में इस क्षेत्र के रुपांतरण पर प्रकाश डाला है। यहां, बौद्ध और मुसलमान ऐतिहासिक रूप से मिल-जुलकर और आपस में एकबद्ध होकर रहते आये हैं लेकिन अब इस क्षेत्र में सीमारेखाओं की मौजूदगी लोगों के आपसी संबंध पर हावी हो गयी है और इससे बहुसंख्यक बौद्ध और अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय के रिश्तों में तनाव पैदा हो रहा है। इलाके में जनसंख्या संबंधी परिवर्तनों का भय बढ़ रहा है तथा बौद्ध और इस्लाम धर्म की एक वैश्वीकृत समझ के बीच दोनों समुदायों के के आपसी तनाव की अभिव्यक्ति इमारतों की भौतिक पुनर्रचना तथा सार्वजनिक स्थानों की व्याख्या के जरिए हो रही है। स्मिथ का अध्ययन ‘सीमा संबंधी संवेदना’ के विकास को दर्शाता है और प्रश्न खड़े करता है कि किस प्रकार सीमाओं द्वारा हाशियाकरण के नये और छद्मघाती स्वरूप निर्मित होते हैं।
विशेषांक के अंतिम शोध-आलेख में हैरिस ने दिखाया है कि किस प्रकार हिमालयी क्षेत्र के सीमांत दायरे के भीतर नये राजनीतिक आर्थिक विकास के कारण हाशियाकरण की स्थितियों में वास्तविक फेरबदल हुआ है। इस फेरबदल के कारण व्यापार के कुछ पुराने स्थान एक किनारे हो गये हैं जबकि इसके साथ ही साथ व्यापार के कुछ नये स्थान खुले हैं तथा कुछ खास तरह की व्यापार प्रक्रियाएं, अप्रकट होने के बावजूद निरंतर जारी हैं। अपने इस अध्ययन के जरिए हैरिस ने हाशियाकरण के विचार को समस्याकृत करते हुए तर्क दिया है कि सीमान्त क्षेत्र में हाशियाकरण की स्थितयां निरंतर परिवर्तनशील और अस्थायी होती है और इस बात का रिश्ता अर्थव्यवस्था, संपर्क-साधन तथा सत्ता के परिवर्तनों से होता है। इसलिए, सुदूर परिधि पर पडा हुआ मान लिए गए इलाकों को अलग-थलग मानने की जगह उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़े हुए क्षेत्र के रुप में विचारने की जरुरत है।