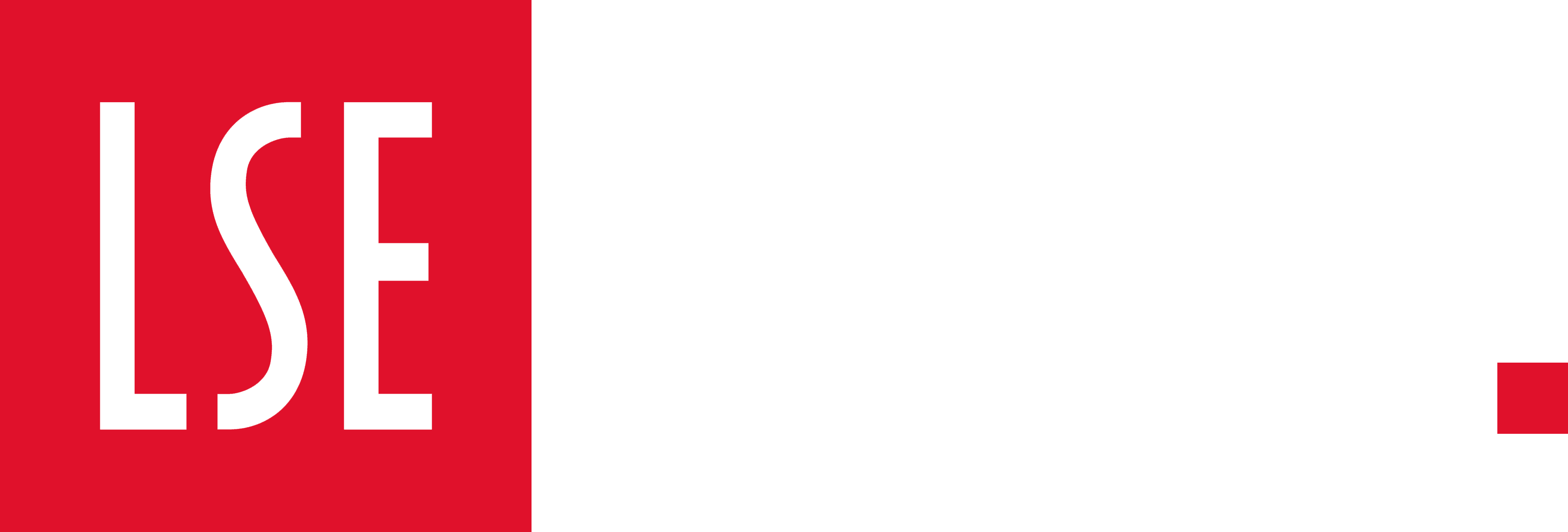Read this post, Top 10 Economic and Development Challenges for India in 2014, in English.
चिरस्थायी विकास: United Nations (संयुक्त राष्ट्र) द्वारा चिरस्थायी विकास को ऐसी प्रक्रिया के तौर पर बताया गया है जो ”अपनी स्वयं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है।” इस वर्ष, भारत पर काम कर रहे अकादमिक जगत के विद्वानों ने प्रश्न किया कि क्या भारत की प्रगति वाकई चिरस्थायी है या क्या शिक्षा व स्वास्थ्य में अधिक निवेश करके और पर्यावरण के लिए हितैषी तरीके से आधारभूत संरचना को विकसित करके, हाल की आर्थिक प्रगति से निर्मित संसाधनों का उपयोग करने में यह देश विफल रहा। 2014 में प्रवेश करते हुए, भारत को बेहतर तरीके से आकलन करना चाहिए कि खाद्य व जल सुरक्षा को बेहतर करने के तरीकों सहित, कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास संबंधी प्रयासों के साथ आर्थिक विकास को किस प्रकार से उन्नत किया जाए।
समावेशी विकास: भारतीय विकास को चिरस्थायी बनाने के लिए, इसे इतना समावेशी होना चाहिए कि यह जातियों (दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी बच्चों व वृद्ध व्यक्तियों सहित), रंग (श्यामवर्ण और गोरे), विकलांगता, लिंग, धर्म (ग्रामीण-शहरी के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों के बीच का अंतर) और कई कारकों के बीच की असमानता से संबंधित समस्याओं को समेट सके। हालांकि नौकरियों और राजनीतिक भागीदारी में लिंग आधारित अंतर कम होता जा रहा है परंतु लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत को खासतौर पर सामाजिक सुरक्षा की नीतियों में सुधार लाकर, समावेशी विकास के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अच्छे उदाहरण जैसे कि ‘अम्मा की उनवागम/कैंटीन’ जिसे हाल ही में तमिलनाडू में शुरू किया गया, जिसमें अत्यधिक सब्सिडी पर पोषक भोजन बेचा जाता है, यह अन्य राज्यों में भी विस्तारित करने योग्य उदाहरण है ताकि कुपोषण के उच्च स्तरों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायता मिले।
जनसांख्यिकीय लाभांश: लगभग 20 करोड़ भारतीय 15 से 24 वर्ष के बीच की आयु के हैं और भारत कामकाजी आयु की बढ़ती हुई जनसंख्या का सर्वाधिक लाभ लेने की अच्छी स्थिति में है। हालांकि जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ लेने के लिए, भारत को कुशलताओं और श्रम की मांग और आपूर्ति का सावधानीपूर्वक प्रबंधनकरना होगा। हालांकि सरकार ने शिक्षा तक पहुंच को बेहतर करने की नीतियां लागू की हैं परंतु शिक्षा के स्तर, अध्यापन के मानकों, परीक्षा के तरीकों, कुशलताओं के विकास, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों आदि को बेहतर बनाने के अभी बहुत अधिक प्रयास किये जाने की जरूरत है। शिक्षा के अधिकार की नीति को प्रभावी बनाने के लिए, देश की सुविधाहीन और सुविधा-संपन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के बीच के अंतर को दूर करने की चुनौतियों को भी संबोधित करना चाहिए ताकि वे मिलजुलकर पढ़ने में सक्षम हो सकें और एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझें, सम्मान करें और एक-दूसरे के मित्र बनें। नये वर्ष में, भारत को सार्वजनिक-निजी भागीदारी और सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रमों को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए जिनसे इस देश की युवा जनसंख्या के लिए आजीविका सुनिश्चित हो सकती है।
मुद्रास्फीति: 2014 के चुनावों से पहले, राजनीतिज्ञों, नीति-निर्माताओं और लोगों के मन में अधिक मुद्रास्फीति का मुद्दा सबसे ऊपर है। पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि 10 प्रतिशत की औसत वार्षिक गति से हुई है और भारतीय लोग अगले वर्ष 13 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और वह उरजित पटेल कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर भारत की मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की समीक्षा करेगा, जिसके द्वारा इस वर्ष के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की उम्मीद है। कृत्रिम रूप से प्रेरित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों (मैकेनिज़म) को नियंत्रित करना भी अनिवार्य है। सेंट्रल बैंक और वित्त मंत्रालय मिलजुलकर काम कर रहे हैं ताकि कारणों का विश्लेषण हो व उन्हें समझा जाए और ऐसे रास्ते निकाले जा सकें ताकि निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके और मुद्रास्फीति पर रोक लगाई जा सके।
तीव्र शहरीकरण: भारतीय शहर अभूतपूर्व रफ्तार से बढ़ रहे हैं — संभावना है कि 2030 तक भारत की शहरी जनसंख्या बढ़कर 59 करोड़ हो जाएगी। इस तीव्र शहरीकरण से आर्थिक विकास को गति मिलने की भी संभावना है: कुछ अनुमानों के अनुसार, 2030 तक शहरों द्वारा 70 प्रतिशत तक नई नौकरियां सृजित की जा सकती हैं और भारतीय जीडीपी का 70 प्रतिशत हिस्सा निर्मित किया जा सकता है। शहरीकरण के आर्थिक फायदे का लाभ लेने के लिए, भारतीय सरकार को बेहतर नीतियां विकसित करनी चाहिए ताकि चिरस्थायी साधनों के माध्यम से शहरी आधारभूत संरचना की जरूरतों को पूरा किया जा सके और बढ़ती हुई शहरी निर्धनता और असमानता की समस्या का समाधान किया जा सके।
भूमि सुधार: इस वर्ष पारित हुए भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर मिली-जुली समीक्षाएं की गईं। ऐसी चिंताएं हैं कि उन किसानों और भूस्वामियों जिनकी जमीनें अधिगृहित की गई हैं, को अनिवार्य रूप से न्याय प्रदान किये बगैर, नये कानून से पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ेंगी और कई औद्योगिक व रियल एस्टेट परियोजनाएं अलाभकारीअव्यवहार्य हो जाएंगी। यह और भूमि सुधार से संबंधित अन्य चुनौतियां — खासतौर पर शहरीकरण और कम आय के शहरी आवास की बढ़ती हुई जरूरतों के संदर्भ में — का मतलब है कि भारत को चिरस्थायी व समान रूप से लाभकारी विकास सुनिश्चित करने के लिए भूमि-संबंधी कानून का मसौदा निरंतर तैयार करते रहना होगा।
केंद्र-राज्य के बीच का संबंध: आर्थिक विकास, प्रशासन और नीतियों को प्रभावित करने में राज्यों की प्रत्यक्ष भूमिका तेजी से अधिक प्रमुखता हासिल करती जा रही है। राज्य स्थानीयता पर आधारित विकास को गति दे रहे हैं, जिस से वे अपने स्वयं के निवेश बढ़ा रहे हैं और ऐसे मॉडल विकसित कर रहे हैं जिनका पूरे देश में अनुकरण किया जा रहा है। परंतु एक राज्य का दूसरे राज्य से परस्पर व्यवहार सुगम बनाने के लिए केंद्र को अधिक प्रयास करने चाहिए और राज्यों को अपनी श्रेष्ठ प्रक्रियाओं की जानकारी उनके बीच में साझा करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। राज्यों के बीचअसमान विकास को संतुलित करने के लिएकेंद्र सरकार को भी अधिक प्रयास करने चाहिएं।
वृद्ध नागरिक: जबकि विकास को गति देने के लिए भारत को अपनी युवा जनसंख्या का पूरा उपयोग करना चाहिए, परंतु इसे वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य और कल्याणकारी सेवाओं पर व्यय बढ़ाने की योजना भी आरंभ कर देनी चाहिए। भारत में प्रजनन दर कम हो रहा है क्योंकि जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है: 2050 तक 30 करोड़ से अधिक भारतीय 60 वर्ष से अधिक आयु के हो जाएंगे। ‘भारतीय कभी रिटायर होते हुए नहीं दिखाई देते’ ऐसा कई क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए कहा जाता है खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी कई लोग कई वर्षों तक काम करना जारी रखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिवर्तित होती हुई जनसंख्या अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, कल्याणकारी सेवाओं और परिवारों के बोझ को बढ़ा देगी। वृद्ध महिलाएं जिनकी संख्या वृद्ध पुरुषों से अधिक होगी, के अधिक अरक्षित स्थिति में रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, भारत में रहने वाले वृद्ध अभिभावकों के संबंध में रोचक अवसर और चुनौतियां उपस्थित होती हैं जब उनके बच्चे विदेश चले जाते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत को यह सुनिश्चित करने वाली नीतियां विकसित करनी चाहिए कि इसके वृद्ध नागरिक भी सवस्थ हों और आनंदकारी जीवन जियें।
भारत-चीन व्यापार: इस वर्ष कई कूटनीतिक अवरोधों के बावजूद, भारत और चीन दोनों सरकारें अगले कुछ वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन के साथ व्यापार करना भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन व्यापारिक संबंध एकतरफा बने हुए हैं जिसमें भारतीय उपभोक्ता चीनी सामान अधिक खरीद रहे हैं जबकि इसकी तुलना में चीनी उपभोक्ता भारतीय सामान कम खरीद रहे हैं। भारत को इसकी निर्यात प्रतियोगी क्षमता को बेहतर करके और चीन के साथ संतुलित व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक सामान, सेवाओं व नीतियों को चिह्नित करके इस नये वर्ष में इस व्यापार घाटे की समस्या का समाधान करना होगा।
भारत-पाकिस्तान व्यापार: पिछले दशक में, भारत-पाकिस्तान व्यापार प्रति वर्ष 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया है। परंतु यह तो सिर्फ शुरुआत है: कुछ अनुमानों के अनुसार, सामान्य स्थिति में द्विपक्षीय व्यापार का आकार 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर जितना अधिक हो सकता है। द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में प्रगति की जिम्मेदारी फिलहाल पाकिस्तान पर निर्भर है: भारत-पाकिस्तान संबंधों को बेहतर करने की बार-बार मांग करने के बावजूद, अभी भी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ जिन्होंने मई में सत्ता संभाली थी, द्वारा भारत को सर्वाधिक वरीयता वाले देश का दर्जा दिया जाना बाकी है। हालांकि जब तक पाकिस्तान यह प्रमुख कदम नहीं उठाता है तब तक व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत के पास करने योग्य कुछ नही हैं परंतु नई दिल्ली को द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए अपना समर्थन देना जारी रखना चाहिए क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी होगा जबकि इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध बेहतर करने में भी मदद मिलेगी।
डॉ रुथ कत्तुमुरी LSE एशिया रिसर्च सेंटर और इंडिया ऑब्ज़रवेट्री की सहनिदेशक हैं।